बंजारा भाषा : आठवी अनुसूची में सम्मिलीत की प्रतिक्षा, बाधाऐ और सुझाव
भारतीय विविधता को समृद्ध करने में जिस जिस भाषा और मौखिक बोलीने महत्वपूर्ण योगदान दिया है उन्हीं में बंजारा भाषा का जिक्र किया जाता है। भलेही वह संविधान की आठवी अनुसूची में सम्मिलीत नहीं हो। भाषा के मान्यता से वंचित रही बंजारा भाषा समय के साथ संघर्ष करके अपनी जड़े मजबुत करती रही यही इसकी विशेषता है
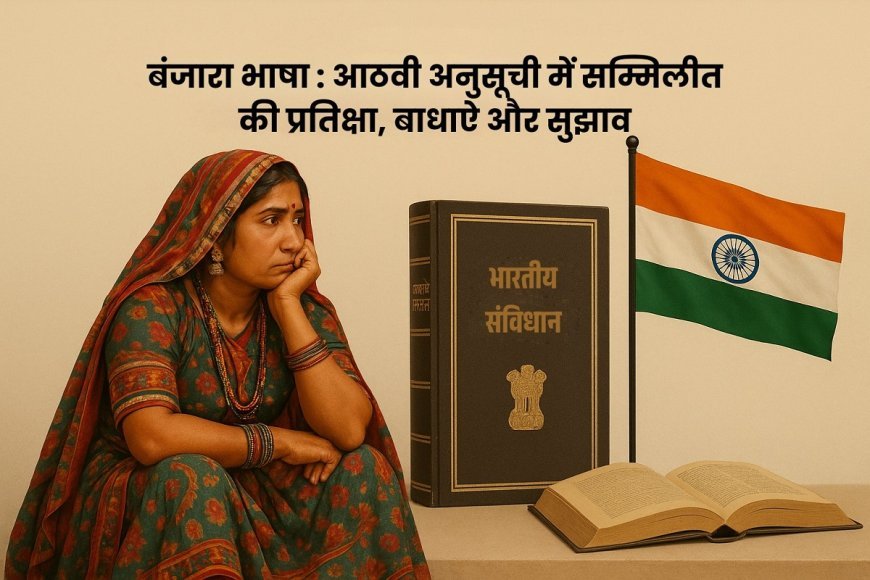
बंजारा भाषा अपनी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही भारतीय विविधता और एकात्मता के लिये भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। यह सदियोंसे समुदाय की परंपराओं, रीति-रिवाजों और अपनेपन की भावनाओ की गहराई से जुड़ी हुई है। बंजारा समाज में, भाषा दिन-प्रतिदिन के संचार के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करती है। बंजारा भाषा ने भारतीय विविधता को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बंजारा समुदाय यूरोपीय देशों के साथ व्यापार करता था, तब भारतीय मूल्यों, शिक्षाओं और यूरोपीय संस्कृति और नवाचार के आदान-प्रदान का प्रभाव होता रहा। अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के साथ बंजारा संस्कृति ने अपनी बंजारा भाषा के माध्यम से वैश्विक नागरिकता की भूमिका को स्पष्ट किया है। बंजारा भाषा, जिसका इतिहास और विरासत हज़ारों साल पुरानी है। देश की विविधताको समृद्ध करने के लिए संविधान के अनुच्छेद आठवी में शामिल किए जाने की ज़रूरत है। लेकिन यह अभी भी भाषा के दर्जा से वंचित है। बंजारा भाषा को भारतीय संविधान की आठवी अनुसूची में शामिल होने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
मानकीकरण और बुनियादी ढाँचे के समर्थन का अभाव : बंजारा भाषा को भारतीय संविधान की आठवी अनुसूची में शामिल होने में कुछ चुनौतियों है, उन्हमें मुख्य चुनौतियों में से एक मानकीकृत लिपि का अभाव है। हालाँकि भाषा में क्षेत्रीय विविधताएँ हैं, लेकिन कोई भी समान लिपि व्यापक रूप से स्वीकार नहीं की गई है। जिससे शैक्षिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भाषा को मानकीकृत करना मुश्किल हो गया है। बंजारा समुदाय अक्सर भाषा लिखने के लिए देवनागरी या रोमन लिपि का उपयोग करता है, लेकिन इसे एक सुसंगत, व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त लेखन प्रणाली में औपचारिक रूप नहीं दिया गया है। बंजारा भाषा का व्यापक रूप से सरकार, शिक्षा और मीडिया जैसी औपचारिक व्यवस्था में उपयोग नहीं किया जाता है, जो इसके प्रदर्शन और संस्थागत समर्थन को सीमित करता है। यह मुख्य रूप से एक मौखिक भाषा है, जिसमें लिखित रूपों पर जोर बहुत कम दिया जाता है। नतीजतन, भाषा में ८वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे (जैसे पाठ्यपुस्तकें, सरकारी दस्तावेज, आदि) का अभाव है।
सामाजिक-आर्थिक उपेक्षाऐ और राजनीतिक वकालत : बंजारा समुदाय, जिसे पारंपरिक रूप से एक खानाबदोश और घुमंतु समूह के रूप में देखा जाता है, अक्सर सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करता है। इस हाशिए पर होने का मतलब है कि अन्य अधिक प्रमुख भाषाई समुदायों की तुलना में उनकी भाषा को शामिल करने की वकालत कम हुई है। सांस्कृतिक या भाषाई संरक्षण के बजाय अस्तित्व और बुनियादी कल्याण पर समुदाय का ध्यान, उनकी भाषा के प्रचार की उपेक्षा में भी भूमिका निभाता है। इसके विपरीत, बंजारा भाषा के पास ८वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक लॉबी या आंदोलन नहीं है। अन्य प्रमुख भाषाओं में अधिक मुखर और अच्छी तरह से समर्थित अभियान हैं, जो अक्सर बंजारा जैसी भाषाओं पर हावी हो जाते हैं, जिनका छोटा या कम संगठित बोली-प्रसार आधार होता है।
जनसांख्यिकी और ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्ष : महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान जैसे विभिन्न राज्यों में बंजारा लोगों के विभिन्न उप-समूहों द्वारा बोली जाने वाली बंजारा भाषा, जिसमें बोलने वालों की संख्या किसी एक क्षेत्र में मुख्य रुप से ज़्यादा नहीं है। समुदाय की बिखरी हुई प्रकृति और भाषा की क्षेत्रीय विविधताएँ मान्यता के लिए एक सुसंगत माँग बनाने के प्रयासों को जटिल बनाती हैं। भाषावार प्रांतरचना होने के कारण बंजारा जैसी बहुसंख्य रुप में होते हुए भी उसे भाषा की मान्यता से वंचित होना पडा। भारत में आठवीं अनुसूची में मान्यता के लिए बड़ी संख्या में भाषाएँ हैं। परिणामस्वरूप, बड़ी आबादी द्वारा बोली जाने वाली या अधिक औपचारिक संस्थाओं (जैसे तमिल, तेलुगु और मराठी) वाली भाषाएँ अक्सर बंजारा जैसी भाषाओं पर हावी हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त, हिंदी, अंग्रेज़ी और क्षेत्रीय भाषाओं जैसी अधिक आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव वाली भाषाएँ आधिकारिक क्षेत्रों पर हावी हो जाती हैं, जिससे बंजारा जैसी कम ज्ञात भाषाएँ ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्ष करती हैं।
भाषाई पहचान के मुद्दे : बंजारा भाषा को बढ़ावा देने के महत्व के बारे में बंजारा समुदाय के भीतर अक्सर आम सहमति का अभाव होता है। कुछ मामलों में, इस बात को लेकर आंतरिक मतभेद हो सकते हैं कि भाषा को एक अलग इकाई के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए या किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा की बोली के रूप में। बंजारा समुदाय द्वारा अभिव्यक्त होनेवाली यह मातृभाषा है, जिसे एकही नाम से संबोधन करना चाहिए, लेकीन जैसे अलग अलग राज्य में बंजारो को भिन्न भिन्न नाम से संबोधन होता है, वैसे ही भाषा को भी भिन्न भिन्न नाम से प्रयोग करना यही उसकी बहुसंख्याक भाषा प्रयोग के मानको पर आघात साबित होती है। संपूर्ण भारतवर्ष मे उसे एकही नाम से संबोधित करना चाहिए।
आठवीं अनुसूची में भाषा को शामिल करना आम तौर पर भाषाई, राजनीतिक और सामाजिक कारकों के संयोजन से प्रभावित होता है। छोटी भाषाओं को मान्यता देने के लिए राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की ओर से मजबूत नीतिगत पहल की अनुपस्थिति बंजारा जैसी भाषाओं के लिए ध्यान आकर्षित करना मुश्किल बनाती है। क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और विकास का समर्थन करने वाले सक्रिय सरकारी ढांचे की अनुपस्थिति बंजारा के समावेश की संभावना को सीमित करती है।
२. एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता। : भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में किसी भाषा को सम्मिलीत करने के लिये कुछ अधिकारिक एवं टेक्निकल क्राइटेरीया होता है। बंजारा समुदाय की काश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग पंद्रह करोड की आबादी है। आज बड़े पैमानो में बंजारा भाषा में लिखित एवं डिजीटल स्वरूप में साहित्य का निर्माण हो रहा है। लेकीन बंजारा भाषा को एक बहुआयामी दृष्टिकोन की आवश्यकता है।
बंजारा भाषा के लिए पैरवी और नीति निर्माण : बंजारा भाषा एक स्वतंत्र और प्राचीन भाषा है। इसलिए इसके संरक्षण और मान्यता के लिए, समाज में साहित्य, संस्कृति और सामाजिक संगठन के क्षेत्रों से मजबूत पहल करने की आवश्यकता है। सांसद हरिभाऊ राठौर, राजीव सातव, उमेश जाधव, कविता नाइक, प्रतिभा धानोरकर, संजय देशमुख ने संसद में बंजारा भाषा का दर्जा दिलाने की मांग की। महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों के बंजारा विधायकों ने अपने विधानसभाओं में लगातार मांग की है। साथ ही, अखिल भारतीय बंजारा सेवा संघ एक सामाजिक संगठन है जो कई वर्षों से इस पर काम कर रहा है। बंजारा भाषा, साहित्य और संस्कृति के विशेषज्ञ एकनाथ पवार नायक ने महाराष्ट्र में पहली बार हस्ताक्षर अभियान चलाया। उन्होंने बंजारा भाषा और बंजारा साहित्य अकादमी के लिए राज्यपाल से मुलाकात की। बलिराम पाटील, आत्माराम राठोड, मोतीराज राठौड, मोहन नाइक, रमेश आर्य, महेशचंद्र बंजारा, विरा राठौड, पंजाब चौहान, एकनाथ पवार, गोवर्धन बंजारा, निलेश राठौड आदि बंजारा साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता का भी बंजारा भाषा की मान्यता के लिए आवाज उठाने में योगदान रहा। इसके साथ ही आज अखिल भारतीय स्तर का साहित्य सम्मेलन भी हो रहा है। यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। लेकिन इन मांगों के लिए एक जन आंदोलन खड़ा करना भी उतना ही जरूरी है।
संसद सदस्यों (सांसद) या राज्य के विधायकों से संपर्क करके पहल करनी होगी, जिनकी बंजारा समुदाय के कल्याण में निहित रुचि है। साथ ही, हमें संसद में बंजारा भाषा की मान्यता की मांग उठाने के लिए उनका समर्थन प्राप्त करना होगा। आठवीं अनुसूची में किसी भाषा को शामिल करने के लिए आमतौर पर भारतीय भाषा सर्वेक्षण या इस उद्देश्य के लिए नियुक्त समितियों की औपचारिक सिफारिश होती है। ऐसे भाषाविदों और विशेषज्ञों को लाएं जो बंजारा भाषा, इसकी बोलियों और इसके ऐतिहासिक महत्व की अनूठी विशेषताओं का दस्तावेजीकरण कर सकें। विशेषज्ञों के शामिल होने से आंदोलन को विश्वसनीयता मिलेगी।
भाषा का मानकीकरण
बंजारा भाषा की लिपि को मानकीकृत करने पर काम करने की वास्तविक आवश्यकता है। जबकि कई बंजारा भाषी रोमन या देवनागरी लिपि बोलते हैं, एक एकीकृत मान्यता प्राप्त लिपि शैक्षिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भाषा को औपचारिक बनाने में मदद कर सकती है। बंजारा भाषा में डिजिटल सामग्री. संदर्भ पुस्तकें, शब्दकोश, वेबसाइट और अन्य शैक्षिक संसाधनों के विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
इससे युवा पीढ़ी को भाषा सीखने और दैनिक जीवन में इसके उपयोग को प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लोक संगीत और कहानी सुनाने के माध्यम से बंजारा भाषा के उपयोग को बढ़ावा दें। सांस्कृतिक कार्यक्रम भाषा के महत्व पर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और लोगों की रुचि पैदा कर सकते हैं। मीडिया एक्सपोजर भाषा की दृश्यता बढ़ाएगा और आधुनिक समाज में इसकी प्रासंगिकता दिखाएगा।
बंजारा लेखक, विशेषज्ञों और भाषाई सहयोग की भूमिका
बंजारा साहित्यिक कृतियाँ, भले ही संख्या में कम हों, एक भाषा को संरक्षित करने और बढ़ावा देने का एक शक्तिशाली साधन हो सकती हैं। अन्य भाषाई समुदायों के साथ जुड़ें जिन्होंने भाषा की मान्यता के लिए संघर्ष किया है, जैसे कि समान सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले समुदाय बंजारा भाषा के महत्व और आधिकारिक मान्यता की आवश्यकता के दावे को पुष्ट करने के लिए ऐतिहासिक रिकॉर्ड, सांस्कृतिक दस्तावेज और समुदाय के सदस्यों से साक्ष्य एकत्र करें। भारत की भाषाई विविधता के संदर्भ में बंजारा भाषा के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने वाले शोध का संचालन करें। नृवंशविज्ञान अध्ययन राष्ट्रीय नीति में भाषा को शामिल करने के लिए एक सम्मोहक मामला बना सकते हैं। बंजारा भाषा बोलने वालों में गर्व की भावना को प्रोत्साहित करें। सांस्कृतिक कार्यक्रम, सार्वजनिक चर्चाएँ और जागरूकता अभियान समुदाय के समर्थन को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। बंजारा भाषा का भाषाई संरक्षण, प्रचार और विकास, विशेष रूप से वैश्वीकरण और भाषाई आत्मसात जैसी आधुनिक चुनौतियों का सामना करते हुए बंजारा मुख्य रूप से एक मौखिक भाषा है, विशेषज्ञ लोकगीतों, कहानियों और ऐतिहासिक आख्यानों जैसी मौखिक परंपराओं को लिखने और संरक्षित करने में मदद करते हैं। यह दस्तावेज़ीकरण भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिकॉर्ड के रूप में काम कर सकता है। विशेषज्ञ भाषा को सीखने वालों के लिए सुलभ बनाने के लिए पाठ्यपुस्तकों, कार्यपत्रकों और शब्दकोशों जैसे शैक्षिक संसाधनों का विकास करते हैं। ये संसाधन मूल वक्ताओं और नए शिक्षार्थियों दोनों को औपचारिक शैक्षिक संदर्भों में भाषा से जुड़ने में मदद करते हैं।
बंजारा भाषा के सामने आने वाली चुनौतियों में से एक मानकीकृत लिपि का अभाव है। बंजारा भाषा के विशेषज्ञ एक सुसंगत लिपि या वर्तनी का प्रस्ताव या विकास कर सकते हैं, जिसका व्यापक रूप से उपयोग किया जा सके। इसमें यह तय करना शामिल हो सकता है कि मौजूदा लिपि (जैसे देवनागरी या रोमन) को अपनाया जाए या एक नई लिपि बनाई जाए। विशेषज्ञ एक मानक ढांचा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिसका उपयोग शैक्षिक सेटिंग्स में किया जा सकता है। इसमें वाक्यविन्यास, आकृति विज्ञान और वाक्य संरचना के लिए नियमों को परिभाषित करना शामिल है।
भाषा विशेषज्ञ और लेखक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में काम करते हैं जो बंजारा भाषा को समुदाय की पहचान के प्रतीक के रूप में बढ़ावा देते हैं। वे एक विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने और बोलने वालों के बीच गर्व को बढ़ावा देने में भाषा के महत्व को उजागर करते हैं। लेखक और विशेषज्ञ साहित्यिक उत्सव और सांस्कृतिक समारोह जैसे कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं जहाँ बंजारा भाषा का उपयोग इसकी सुंदरता और प्रासंगिकता को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।
४. बंजारा भाषा की अनूठी भाषाई विशेषताएँ और महत्व
बंजारा भाषा एक अनुठी मातृभाषा है। 'बंजारा भाषा यह ग्लोबल सिटीझन की चौदहखड़ी की उपदेश देती है। वह एक सहिष्णु है, उसमें किसी प्रकार का द्वेषभाव नहीं मानवीय रिश्ता संजोगनेवाली हृदय की बोली है। जो प्रकृति के गोद में खिलनेवाली प्रकृति की बोली है।' हर बंजारो को वह अपनी माँ के समान प्यारी और खुबसुरत प्रतित होती है।
सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधताएँ
बंजारा एक एकल, एकरूप भाषा नहीं है, बल्कि समुदाय के विभिन्न उपसमूहों द्वारा बोली जाने वाली कई बोलियों से मिलकर बनी है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, गोवा और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में भाषा अलग-अलग है। ये बोलियाँ स्थानीय प्रभावों को दर्शाती हैं, जिनमें अक्सर तेलुगु, मराठी, हिंदी, गुजराती और कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं के तत्व शामिल होते हैं। बंजारा भाषा में विशेष शब्दावली शामिल है जो समुदाय की खानाबदोश और देहाती जीवनशैली को दर्शाती है। इसमें व्यापार, यात्रा और पशुपालन से संबंधित शब्द शामिल हैं, जो आम तौर पर मुख्यधारा की भारतीय भाषाओं में नहीं पाए जाते हैं। बंजारा भाषा की अपने आप में एक स्वंय विशेषताऐ है।
सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण
बंजारा भाषा समुदाय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए एक वाहक के रूप में कार्य करती है। मौखिक परंपराओं, लोककथाओं, कहावतों, गीतों और कहानियों के माध्यम से, भाषा सदियों पुराने ज्ञान, विश्वासों और मूल्यों को वहन करती है जो बंजारा लोगों के अद्वितीय सांस्कृतिक ताने-बाने को परिभाषित करते हैं। बंजारा भाषा का उपयोग सामुदायिक पहचान की मजबूत भावना को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह साझा इतिहास के प्रतीक के रूप में कार्य करता है, जो क्षेत्रीय सीमाओं को पार करने वाले एक सामान्य भाषाई और सांस्कृतिक धागे के माध्यम से व्यक्तियों को जोड़ता है। बंजारा भाषा केवल संचार का एक तरीका नहीं है, बल्कि पहचान का एक चिह्न है, जो बंजारा लोगों को अन्य | समुदायों से अलग करती है। ऐसे समाज में जहाँ भाषा अक्सर सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाती है, बंजारा भाषा उनकी विशिष्टता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
ऐतिहासिक और मौखिक परंपरा
बंजारा साहित्य का अधिकांश भाग मौखिक रूपों में मौजूद है, जैसे 'गीत, गाथागीत और महाकाव्य'। ये मौखिक परंपराएँ बंजारा लोगों के इतिहास, रीति-रिवाजों और सामाजिक मानदंडों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। कहानी और गीतों के माध्यम से, बंजारा भाषा उनकी खानाबदोश जीवनशैली, सामाजिक संरचनाओं और प्रकृति के साथ संबंधों के बारे में ऐतिहासिक आख्यान प्रस्तुत करती है। बंजारा भाषा समुदाय की ऐतिहासिक यात्रा, भारत के विभिन्न हिस्सों में उनके प्रवास, उनके संघर्ष और समाज में उनके योगदान को दर्ज करने में मदद करती है। साहित्य के माध्यम से, इन कहानियों को संरक्षित किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आने वाली पीढ़ियाँ समुदाय के अतीत और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय इतिहास को आकार देने में इसकी भूमिका को समझें।
सामाजिक और नैतिक मूल्यों का संरक्षण
बंजारा भाषा में निहित कहावतें, सूक्तियाँ और नैतिक शिक्षाएँ सामाजिक मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों को आकार देने में आवश्यक हैं। ये भाषाई रूप परिवार, रिश्तों, बड़ों के प्रति सम्मान और समुदाय के मूल नैतिक सिद्धांतों के बारे में ज्ञान संचारित करते हैं। बंजारा भाषा समुदाय के भीतर भक्ति प्रथाओं का केंद्र है। धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों का हिस्सा बनने वाले कई गीत, प्रार्थनाएँ और भजन बंजारा में हैं, जो समुदाय के आध्यात्मिक जीवन को मजबूत करने में मदद करते हैं। ये धार्मिक ग्रंथ देवताओं के प्रति भक्ति, दैवीय हस्तक्षेप की कहानियाँ और समुदाय के नैतिक दिशा-निर्देशों का मार्गदर्शन करने वाली शिक्षाएँ देते हैं।
सशक्तिकरण के साधन के रूप में भाषा
मातृभाषा अपने समुदाय के लिये गर्व का स्त्रोत है। जैसे-जैसे समुदाय तेजी से आधुनिक होती दुनिया में चुनौतियों का सामना कर रहा है, भाषा सांस्कृतिक क्षरण और भाषाई आत्मसात के खिलाफ प्रतिरोध के साधन के रूप में कार्य करती है। यह समुदाय को बाहरी दबावों का सामना करने में अपनी पहचान का दावा करने का अधिकार देती है। भाषा पुनरोद्धार आंदोलन बंजारा समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों, जैसे सामाजिक हाशिए पर होना और अपनी मूल भाषा में शिक्षा तक पहुँच की कमी की ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। इस प्रकार भाषा मान्यता अधिक सामाजिक समानता प्राप्त करने के साधन के रूप में काम कर सकती है। बंजारा भाषा भारत के विशाल भाषाई परिदृश्य को इसकी | विविधता में योगदान देकर समृद्ध करती है। अल्पसंख्यक भाषा के रूप में, बंजारा भारत के बहुभाषी ताने-बाने और कम ज्ञात भाषाओं के संरक्षण के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इसकी मान्यता की वकालत करने से भारत की सांस्कृतिक धाराऐ के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में स्वदेशी भाषाओं को संरक्षित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जा सकता है।
निष्कर्ष: बंजारा भाषा की मान्यता के लिए कई मोर्चों पर रणनीतिक और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। सामुदायिक संगठन और सांस्कृतिक प्रचार संस्थागत समर्थन और सरकारी पैरवी के साथ जमीनी स्तर पर लामबंदी को जोड़कर, बंजारा भाषा को अधिक मान्यता और अंततः भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए तैयार किया जा सकता है। हालाँकि, इसके लिए बंजारा समुदाय और बाहरी सहयोगियों दोनों की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी जो भाषाई विविधता और सांस्कृतिक संरक्षण के बारे में भावुक हैं।
जबकि बंजारा भाषा का समुदाय के लिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है, कई कारक जिसमें एक मानकीकृत लिपि की कमी, सीमित संस्थागत समर्थन, राजनीतिक हाशिए पर होना और बड़ी भाषाओं से प्रतिस्पर्धा शामिल है। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में इसके शामिल होने में पर्याप्त बाधाएँ हैं। बंजारा भाषा अपनी भाषाई विशेषताओं, मौखिक परंपराओं, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों और सामाजिक संदर्भों में विशिष्ट है। इसकी अनूठी शब्दावली, द्वंद्वात्मक विविधताएँ और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ एकीकरण इसे एक विशिष्ट भाषाई इकाई बनाते हैं। हालाँकि, मानकीकरण की चुनौतियाँ, सीमित लिखित दस्तावेज़ीकरण और प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं का दबाव इसकी पूर्ण मान्यता और संरक्षण में बाधाएँ पेश करते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, बंजारा भाषा समुदाय की पहचान और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है, जिसकी समृद्धि मौखिक साहित्य के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से व्यक्त की जाती है। बंजारा लेखक, साहित्यकार और बंजारा महिलाएँ और साहित्यकार केवल भाषा को संरक्षित करने में योगदान देते हैं, बल्कि सांस्कृतिक राजदूत के रूप में भी काम करते हैं, जो बंजारा को पुनर्जीवित और आधुनिक बनाने के लिए काम करती हैं। जिससे यह भारत की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रयास आवश्यक हैं कि बंजारा भाषा २१ वीं सदी में भी फलती-फूलती रहे और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचे। बंजारा भाषा सिर्फ़ संचार के साधन से कहीं ज़्यादा है; यह बंजारा समुदाय की विरासत का एक जरूरी हिस्सा है और उनके साहित्यिक और सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय विविधता को समृद्ध करते हुए, वैश्विक भाईचारा, वैश्विक नागरिकत्व का भी संदेश देती है। इस विरासत को संजोगना होगा। इसलिये बंजारा भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलीत करना अवश्य है।

एकनाथ पवार नायक
बंजारा भाषा और संस्कृति विशेषज्ञ एवं साहित्यिक, नागपुर, महाराष्ट्र







